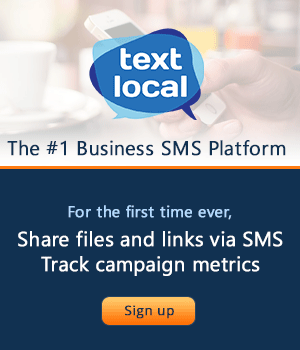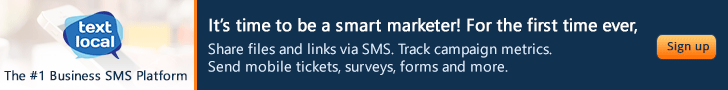समय आ गया है, राजनीतिक दलों को लोकलुभावन वादे जैसे विषय पर विशद चर्चा करना चाहिए. आने वाले आम चुनाव के पहले इस विषय पर एकमत होना जरूरी है. यूँ तो इस विषय पर आर्थिक भर वहन करने वाले में चर्चा लंबे समय से चली आ रही है. हाल ही में सर्वाेच्च न्यायालय की टिप्पणी ने इस पर नये सिरे से बहस शुरू की है. इस विषय की विवेचना से पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में वादे करने और उन वादों पर जनता के फैसले की अहमियतके साथ इससे राज्यों पर आते खर्च के बोझ का हिसाब लगाना जरुरी है.
यह अधिकार सभी दलों को है कि वे लोकहित में जो अच्छा समझें, उसे जनता के सामने रखें. यहाँ यह सवाल उठता है कि लोकलुभावन का अर्थ क्या है? अभी तक इसकी कोई सर्वमान्य या स्थापित परिभाषा नहीं है. दुनियाभर की कल्याणकारी व्यवस्थाओं में ऐसी मदद दी जाती है. यह उन देशों में भी किया जाता है, जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न व समृद्ध हैं. अनेक देशों में स्वास्थ्य व शिक्षा निशुल्क है. ऐसी सुविधाएं हर नागरिक के लिए हैं, चाहें उनकी आर्थिक स्थिति जो हो. इसके विपरीत भारत में ऐसी योजनाएं आम तौर पर गरीबी रेखा से नीचे और बेहद कम आय के लोगों के लिए हैं.ऐसे में यह बात स्वाभाविक है कि जो देश राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से हमसे आगे माने जाते हैं, क्या वे और उनकी पार्टियां लोगों को लुभाने में लगी हुई हैं?
क्या भारत में ऐसी योजनाओं और वादों का गलत राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? अदालत ने साफ कर दिया है कि यह सब वोट ‘खरीदने’ की कवायद है?
सब जानते हैं कि गणतंत्र में वही होगा, जो राजनीतिक दल चाहेंगे, परन्तु यहाँ यह होना चाहिए जो जनता चाहेगी. तर्क के लिए मान लें कि किसी पार्टी ने कुछ वादे किये, पर जनता ने उसे नहीं चुना, तो उसका मतलब यह हुआ कि वे कथित फ्रीबीज लागू नहीं होंगे. इस प्रक्रिया पर कोई रोक तभी लग सकती है, जब वादे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रावधानों के अनुरूप या विपरीत हों. राजनीतिक दलों को ही तय करना चाहिए कि वह जनता से क्या वादा करे और क्या नहीं? ऐसे में सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए साथ ही ऐसे मामलों में अदालतों का अधिकार क्षेत्र क्या होगा? इस पर भी बात होनी चाहिए.
भारत के कई राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है और वे कर्ज में डूबे हुए हैं. उनके संबंध में सबसे पहले यह समझा जाना चाहिए कि कितना वित्तीय दबाव इन कल्याणकारी योजनाओं से आ रहा है और कितना अन्य खर्च है. कई तरह के अनुदान जारी हैं. ऐसी योजनाओं को इसलिए बंद नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकार कर्ज में है. जैसे प्राथमिक शिक्षा पर बहुत खर्च होता है. न्यायपालिका पर भी राज्यों का भारी खर्च है.
भारत में खर्च की कई श्रेणियां हैं. आज भारत में उद्योग जगत को अनेक अनुदान और छूट देने की नई व्यवस्था शुरू हुई है. भारत के सरकारी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में बहुत कम शुल्क लिया जाता है. जो शिक्षा के वास्तविक खर्च से कई गुना अधिक है, निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थानों से तुलना करके देखिये. शिक्षा के प्रति सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से यह जरूरी भी है. इस आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जा सकता.
यह पूरा मसला जटिल है, यह ठीक है कि कुछ राज्यों ने बिना अधिक सोचे-विचारे महत्वाकांक्षी सामाजिक योजनाएं, जैसे एक-दो रुपये में अनाज देना आदि, चलायीं, साथ ही राज्यों की अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए दूसरे कारण अधिक जिम्मेदार हैं. उदाहरण के लिए दो राज्यों - केरल और पश्चिम बंगाल को देखें, जो सबसे अधिक दबाव वाले राज्यों में शामिल हैं. राज्य आमदनी होने पर ही खर्च कर सकेंगे. इन राज्यों में औद्योगिकीकरण खस्ताहाल है. ऐसे में गरीबी बहुत अधिक है, तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी.
कोरोना महामारी के दौर में केरल में जो दूसरे देशों से आमदनी आती थी, वह बहुत हद तक कम हो गयी. इससे उपभोक्ता अर्थव्यवस्था चरमरा गयी और कराधान भी घट गया. ऐसी स्थिति के लिए कल्याण योजनाओं को न दोष देकर भारत को ऐसे राज्यों की आर्थिक नीति एवं स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए तथा उसमें सुधार के प्रयास करने चाहिए.
गरीबों को तो मदद देनी ही पड़ेगी, पर कहाँ तक ? इस मसले पर राजनीतिक स्तर पर बहस भी हो सकती है कि कौन-सी फ्रीबीज या इंसेंटिव सही है और कौन-सी योजना गलत है. इस बहस का अंतिम फैसला चुनाव के पहले सर्व सम्मति से तय हो. सभी राजनीतिक दल आपसी सहमति बना कर चुनाव पूर्व आदर्श आचार संहिता में संशोधन कराएं. भारत में असंतोष बढ़ रहा है.
तय कीजिये कौन से लोकलुभावन वादे लोकहित में हैं. 2 अगस्त. राकेश दुबे, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल.
Category : आजाद अभिव्यक्ति | Sub Category : सभी Posted on 2022-08-02 03:05:07

Contact:
Editor
ओमप्रकाश गौड़ (वरिष्ठ पत्रकार)Mobile: +91 9926453700
Whatsapp: +91 7999619895
Email:gaur.omprakash@gmail.com
Latest Videos
जम्मू कश्मीर में भाजपा की वापसी
बातचीत अभी बाकी है कांग्रेस और प्रशांत किशोर की, अभी इंटरवल है, फिल्म अभी बाकी है.
बातचीत अभी बाकी है कांग्रेस और प्रशांत किशोर की, अभी इंटरवल है, फिल्म अभी बाकी है.
Search
Categories
Recent News
-
दिल्ली में कसा केजरीवाल पर केन्द्र सरकार का फंदा (8 अगस्त) - [
मेरी बात - ओमप्रकाश गौड़ ] -
महिला लापता होने पर राजनीति नहीं, सामाजिक विमर्श कीजिये. 2 अगस्त राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार भोपाल. - [
आजाद अभिव्यक्ति ] -
फिर जला हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहा जाने वाला मेवात 2 अगस्त. - [
मेरी बात - ओमप्रकाश गौड़ ] -
भारी पड़ेगी ज्ञानवापी की लड़ाई 29 जुलाई 2023 - [
मेरी बात - ओमप्रकाश गौड़ ] -
पंजाब को दिल्ली की तरह केन्द्र के साथ टकराव की राह पर ढकेलते भगवंत मान 1 मार्च 2023 - [
मेरी बात - ओमप्रकाश गौड़ ] -
युवतियों की शादी की उम्र पर सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा पल्ला 22 फरवरी 2023 - [
मेरी बात - ओमप्रकाश गौड़ ] -
बुरे फंस गये हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे 22 फरवरी 2023 - [
मेरी बात - ओमप्रकाश गौड़ ] -
नीतीश नहीं छोड़ेगे सीएम की कुर्सी 22 फरवरी 2023 - [
मेरी बात - ओमप्रकाश गौड़ ]